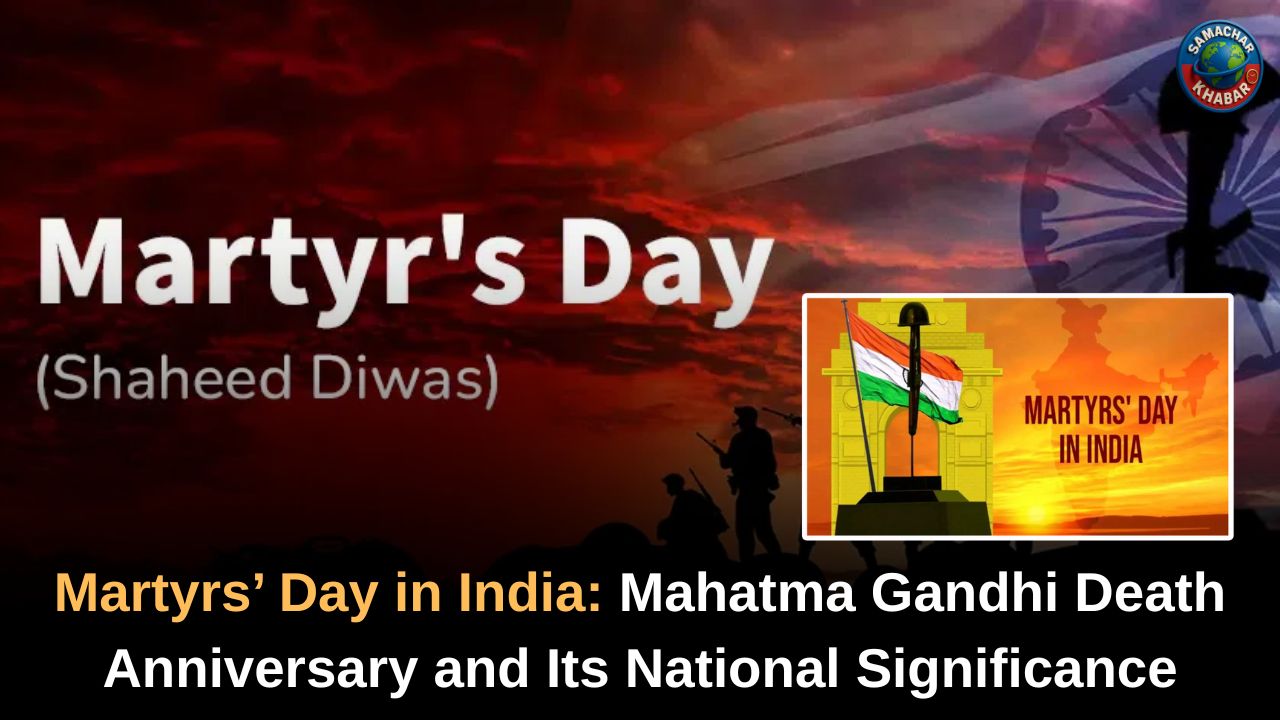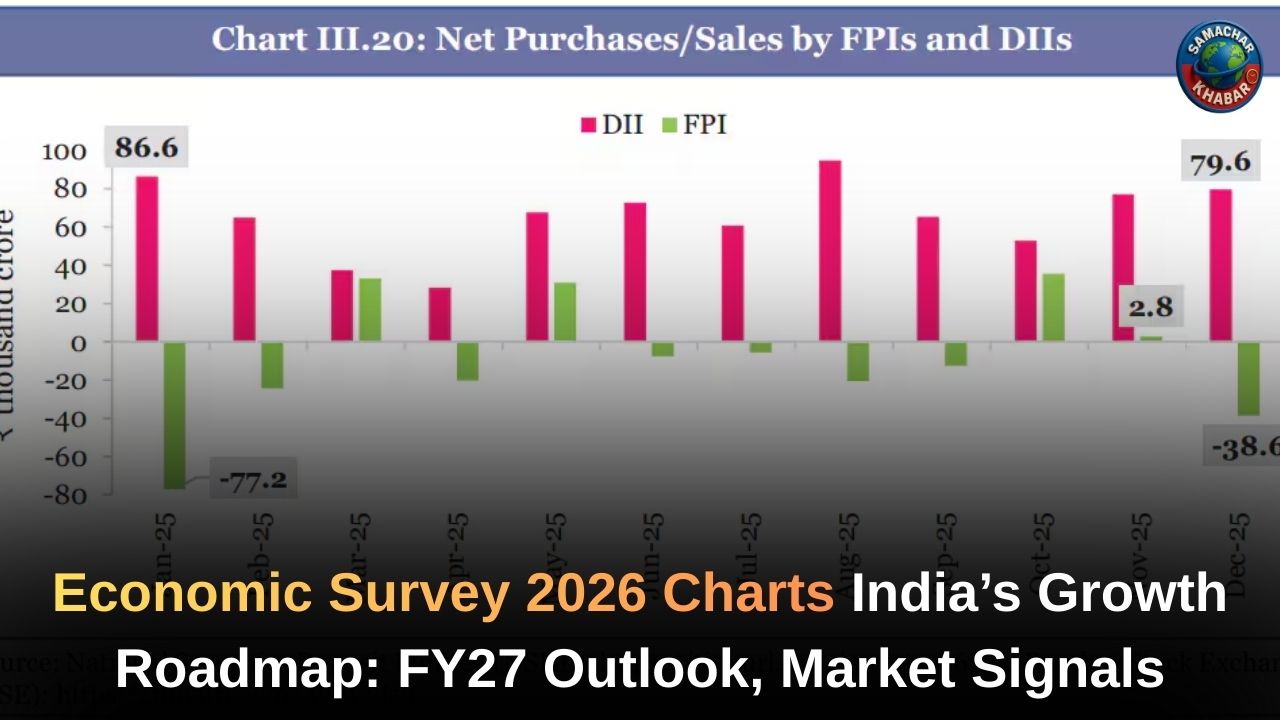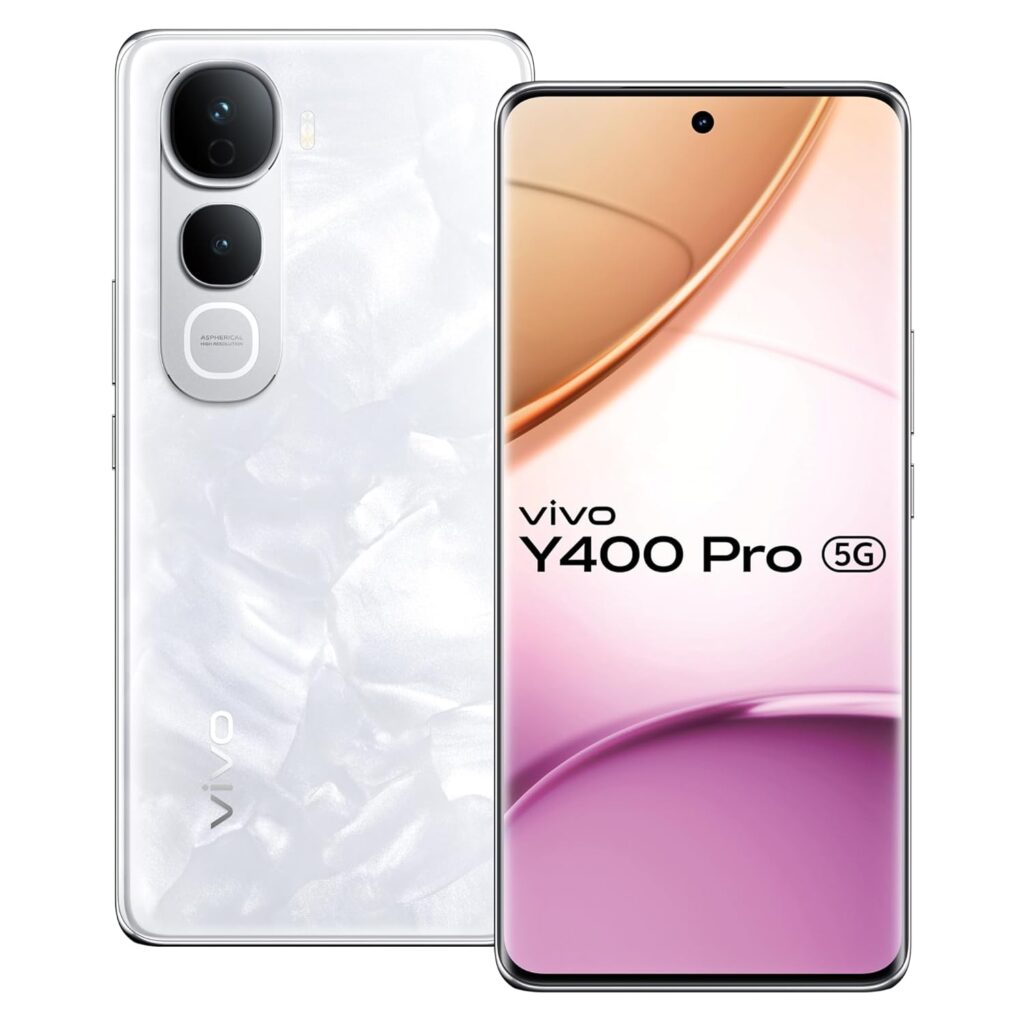हर साल सर्दियों में, दिल्ली-एनसीआर की हवा सांस लेने लायक नहीं रह जाती। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि सरकार को आपातकालीन उपाय करने पड़ते हैं। इन उपायों में से एक है निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध। लेकिन, यह प्रतिबंध न केवल अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उन लाखों दिहाड़ी मजदूरों की रोजी-रोटी भी छीन लेता है जो इन निर्माण स्थलों पर काम करते हैं। यही वह मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है: प्रदूषण का हल निकालो, मजदूरों की रोजी-रोटी मत छीनो…।
इस ब्लॉग पोस्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के पीछे के कारणों को समझेंगे, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की जटिल समस्या पर गहराई से विचार करेंगे, और उन वैकल्पिक समाधानों की तलाश करेंगे जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी मजदूरों के जीवन को प्रभावित न करें।
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का रुख: प्रतिबंध बनाम स्थायी समाधान
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Commission for Air Quality Management (CAQM) को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या के लिए वैकल्पिक समाधान खोजे, बजाय इसके कि हर साल निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे प्रतिबंध मजदूरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिबंध एक अस्थायी समाधान है, और हमें ऐसी स्थायी रणनीतियों पर काम करने की जरूरत है जो प्रदूषण को जड़ से खत्म करें। उन्होंने कहा कि “रोक लगाने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक संकट पैदा करती है।” कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन मजदूरों को पहले मुआवजा देने की बात कही गई थी, उन्हें भी सही समय पर और पूरा मुआवजा नहीं मिला।
यह टिप्पणी इस बात का प्रमाण है कि न्यायपालिका अब सिर्फ तात्कालिक कदमों पर नहीं, बल्कि एक संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण पर जोर दे रही है। इसका मतलब है कि सरकारों को अब प्रदूषण के लिए ऐसे उपाय खोजने होंगे जो सभी हितधारकों, विशेषकर कमजोर तबके के लोगों के हितों का ध्यान रखें।
प्रदूषण का मूल कारण: सिर्फ पराली नहीं, और भी हैं कई गुनहगार
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का मुख्य कारण सिर्फ पराली जलाना नहीं है, जैसा कि अक्सर माना जाता है। यह एक बहुआयामी समस्या है जिसके कई कारक हैं। इनमें शामिल हैं:
- वाहनों से निकलने वाला धुआं: दिल्ली में लाखों गाड़ियां चलती हैं, जिनमें से पुरानी डीजल गाड़ियां प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत हैं।
- औद्योगिक उत्सर्जन: आसपास के राज्यों में स्थित कारखानों से निकलने वाला धुआं और रसायन हवा को जहरीला बनाते हैं।
- धूल और निर्माण कार्य: अनियंत्रित निर्माण और तोड़फोड़ से उड़ने वाली धूल हवा में PM2.5 और PM10 के कणों को बढ़ाती है।
- पराली जलाना: सर्दियों में हरियाणा और पंजाब के खेतों में पराली जलाने से उठने वाला धुआं दिल्ली की हवा को और भी खराब कर देता है।
- जलवायु और भौगोलिक कारक: दिल्ली एक भू-आवेष्ठित क्षेत्र है, जहां सर्दियों में हवा की गति धीमी हो जाती है, जिससे प्रदूषक एक जगह जमा हो जाते हैं।
ये सभी कारक मिलकर एक ‘कॉक्टेल’ बनाते हैं जो दिल्ली-एनसीआर की हवा को ‘खतरनाक’ स्तर तक ले जाता है। एक अध्ययन के अनुसार, दिल्ली के सर्दियों के प्रदूषण में लगभग 64% हिस्सा बाहरी स्रोतों से आता है। यह दर्शाता है कि यह सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं, बल्कि एक क्षेत्रीय मुद्दा है जिसके लिए राज्यों के बीच सहयोग जरूरी है।
मजदूरों की पीड़ा: जब पेट भरने का सवाल हो
निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध का सबसे बुरा असर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ता है। ये वे लोग हैं जो अक्सर बिहार, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान जैसे राज्यों से आते हैं। उनकी आय दैनिक मजदूरी पर निर्भर करती है। जब काम रुकता है, तो उनकी आय का एकमात्र स्रोत बंद हो जाता है।
राजू सिंह, एक राजमिस्त्री, बताते हैं: “जब वे हमारा काम बंद कर देते हैं, तो हमें सिर्फ मजदूरी का नुकसान नहीं होता। हमारी थाली से भोजन छिन जाता है और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो थोड़ी बहुत बचत करते हैं, वो भी गंवा देते हैं।”
सरकार ने हालांकि मुआवजा देने की घोषणा की है, लेकिन कई मामलों में यह मुआवजा या तो देरी से मिलता है या मजदूरों तक पहुंचता ही नहीं। 2024 में, दिल्ली सरकार ने लगभग 90,000 पंजीकृत श्रमिकों को 8,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया था, लेकिन कई रिपोर्टों में यह पाया गया कि यह राशि पर्याप्त नहीं थी और इसका वितरण भी सुचारू नहीं था।
Also Read: दिल्ली में डीजल गाड़ी वालों के मजे ही मजे: सुप्रीम कोर्ट का नया नियम
यह एक गंभीर मानवीय संकट है। प्रदूषण का समाधान खोजते समय, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका सबसे बड़ा बोझ उन लोगों पर पड़ रहा है जो पहले से ही सबसे कमजोर हैं।
आगे का रास्ता: क्या हैं प्रदूषण के स्थायी और मानवीय हल?
सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा है। इस कार्ययोजना में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:
- प्रौद्योगिकी का उपयोग:
- एंटी-स्मॉग गन: निर्माण स्थलों पर धूल को कम करने के लिए एंटी-स्मॉग गन का उपयोग अनिवार्य किया जाए।
- ग्रीन कवर: निर्माण स्थलों को पूरी तरह से हरे कपड़े से ढका जाए।
- वैक्यूम क्लीनिंग: सड़कों की नियमित वैक्यूम क्लीनिंग और पानी का छिड़काव किया जाए।
- सरकारी नीतियां और उनका कार्यान्वयन:
- वाहन प्रदूषण नियंत्रण: बीएस-VI मानकों को सख्ती से लागू किया जाए और पुरानी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुलभ और आकर्षक बनाया जाए।
- पराली का समाधान: पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए। पराली को बायोमास ईंधन में बदलने जैसे वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा दिया जाए।
- अंतर-राज्यीय सहयोग: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर एक एकीकृत प्रदूषण नियंत्रण योजना बनाई जाए।
- मजदूरों की सुरक्षा:
- वैकल्पिक रोजगार: निर्माण पर प्रतिबंध के दौरान मजदूरों के लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, जैसे कि शहरी हरियाली और बुनियादी ढांचे के रखरखाव का काम।
- प्रभावी मुआवजा प्रणाली: एक पारदर्शी और प्रभावी तंत्र बनाया जाए ताकि प्रतिबंध के दौरान प्रभावित मजदूरों को समय पर और पर्याप्त मुआवजा मिल सके।
समाधान के लिए मिलकर काम करना होगा
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह हमें याद दिलाती है कि पर्यावरण की लड़ाई सिर्फ हवा को साफ करने की नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर तबके के जीवन की गरिमा को बनाए रखने की भी है। प्रदूषण का हल निकालो, मजदूरों की रोजी-रोटी मत छीनो… यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि सरकारों, नीति-निर्माताओं और आम जनता के लिए एक नैतिक दायित्व है।
हमें तात्कालिक प्रतिबंधों से आगे बढ़कर स्थायी और समावेशी समाधानों की ओर बढ़ना होगा। यह तभी संभव है जब सभी हितधारक मिलकर काम करें – सरकार, उद्योग, किसान, मजदूर, और नागरिक। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें, तो हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हवा भी साफ हो और किसी का पेट भी भूखा न रहे।